चतुर्थ अध्याय
आपः का एकत्व और अनेकत्व
निघण्टु के उदकनामों में परिगणित आपः शब्द वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शब्द लौकिक संस्कृत में वेद के समान ही सर्वत्र बहुवचन ही प्रयुक्त है। व्याकरण में भी अन्य शब्दों के समान इस शब्द के एकवचन और द्विवचन रूप नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि वेद में आपः प्राणों के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हैं[1] और प्राण सर्वत्र नानारूपात्मक ही हैं, जो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान नाम से सुने जाते हैं, उनमें से कोई भी अकेला नहीं, सब एक दूसरे पर आश्रित होने से, उनमें से किसी का भी स्वतन्त्र एकत्व नहीं है।
सलिल महत् और नाम
फिर भी एक उदकनाम (आपः) को प्राणो का प्रतीक बनाकर, वेद ने उन प्राणों के एकत्वपरक उद्गम की ओर संकेत किया है। ब्राह्मण-ग्रन्थ कहते हैं कि प्राणरूप आपः की धाराएं आदि में ‘सलिल‘ थीं।[2] सलित को ही कभी-कभी मह्त् भी कहा गया है।[3] अतएव निघण्टु में उदकनामों में आपः के साथ ‘सलिल‘ तथा ‘महत्‘ को भी सम्मिलित कर लिया गया। सलिलं के ही रूपान्तरों ‘सलिलानी‘ को आपः कहा जाता है, जिनमें समुद्र ज्येष्ठ है, परन्तु इस कथन द्वारा वेद जिन आपः की ओर संकेत कर रहा है, वे सामान्य सलिल (जल) के रूपान्तर नहीं हैं, अपितु ‘प्राणाः वा आपः द्वारा संकेतित ‘आपः देवीः‘ हैं, जिन्हें वज्री इन्द्र ने अनेकत्व प्रदान किया है।[4] जिस सलिल के मध्य से ये अनेक धाराएं चली आ रही हैं, वह वस्तुतः इन्द्र का ही ‘महत्‘ नामक गुह्य नाम है, जो अनेकत्व भी ग्रहण कर सकता है।[5]
निस्सन्देह, यहाँ जिस ‘नाम‘ का उल्लेख है, वह लौकिक संस्कृत का नाम शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि यह महत् है और गुह्य है तथा सलिलं के समान ‘सलिलानि‘ जैसा अनेकत्व ग्रहण करने वाला है। इसलिए महत् और सलिलं के साथ ‘नाम‘ शब्द का भी समावेश निघण्टु के उदकनामों में है। महत् शब्द पर ध्यान देते हुए डा० फतहसिंह ने अपने ‘वैदिक दर्शन‘ में महत् (सलिलं) के आधार पर ही सांख्य दर्शन के ‘महत्‘ को कल्पित माना है। इस महत् से उद्भूत अहंकार, मन तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर अथर्ववेद ने जिस ‘अष्टाचक्र‘ सृष्टिचक्र की कल्पना की है, वह वस्तुतः देवीः आपः‘ नामक प्राणों का ही सृष्टिचक्र है-
अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा।
अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः।। अथर्व ११,४,२२
इस मन्त्र में निम्नलिखित बिन्दु विशेष रूप से ध्यातव्य हैं--
(१) अष्टाचक्र ‘सहस्राक्षर‘ है। इसका अभिप्राय है कि इसी अष्टविध सृष्टिचक्र के द्वारा नाना प्रकार की इच्छाओं, भावनाओं, विचारों, क्रियाओं आदि की सृष्टि होती है। यही सहस्राक्षरा वाक् की सृष्टि ‘सलिलानि‘ कही गई है, जो अपने मूल पद सहित उक्त अष्टचक्रों को जोड़कर नवपदी[6] होती कही जाती है। इस सहस्राक्षरा वाक् के जो अनेक समुद्र हैं, उनके विविधरूपेण क्षरण करने के कारण चारों दिशाओं को जीवन मिलता है और उन समुद्रों के माध्यम से ही वह क्षरणरहित मूलभूत अक्षरपद भी क्षरण करता है, जिसके सहारे विश्व जीवन धारण करता है[7]।
(२) अष्टाचक्र को एकनेमि कहा गया है, क्योंकि यह चक्र जिन उक्त अष्टप्राणों की संहति का प्रतीक है, वह उक्त एकपदी वाक् की परिधि के अन्तर्गत है। इसी वाक् को ‘प्राणानामुत्तमा‘ ज्योति कहा जाता है[8]।
(३) यह अष्टाचक्र पुरस्तात् और पश्चात् गति करने वाला है, क्योंकि यह वस्तुतः प्राणचक्र है और प्राण को सम़ञ्चन तथा प्रसारण नामक द्विविध गति वाला बताया गया है[9]। इसी द्विविध गति को प्राणरूप हंस के दो पाद माना गया है, जिनमें से एक सदा ही ‘सलिल‘ (महत्) से सम्बद्ध रहता है अर्थात् या तो सलिलं फैले हुए नानात्व का समञ्चन एकत्व में करता है या एकत्व को पुनः नानात्व में प्रसारित करता है। इन दानों पादों को उठा लेने का अर्थ होगा कि अद्य, श्व अहोरात्र तथा उषा काल के रूपक द्वारा वर्णित नानात्व सृष्टि का सर्वथा अभाव, जिसके फलस्वरूप यह हंस पूर्वोक्त उस अक्षर में परिणत हो जायेगा जो नानारूपात्मक सृष्टि रूपी क्षरण से सर्वथा रहित है--
एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद् हंस उच्चरन्।
यदङ्ग स समुत्खिदेत् नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री न व्युच्छेत् कदाचन।।- अथर्व ११.४.२१
4. विश्वभुवन के नानात्व की सृष्टि करने वाला उक्त चक्र वस्तुतः किसी मूलभूत तत्त्व का अर्धभाग ही है, परन्तु अवशिष्ट अर्धभाग एक अज्ञात रहस्य है। इस रहस्य का उद्घाटन, यहां प्रथम बिन्दु की व्याख्या में उल्लिखित वह सत्य ‘अक्षर‘ (क्षरणरहित) करता है जो उक्त ‘अष्टाचक्र एकनेमि के माध्यम से क्षरण करता है। डा० फतहसिंह के अनुसार यह ‘अक्षर‘ वह ऊॅ ब्रह्म है, जिसे वेदान्त में निर्गुण ब्रह्म तथा आगमों में परम शिव कहा गया है। यह शक्तिमान शिव का वह रूप है, जिसमें उसकी शक्ति लीन रहती है। इस अक्षर के क्षरण होने का अर्थ है, उसमें प्रतिष्ठित आपः रूप उसकी शक्ति का नानारूपात्मिका होकर सृष्टि करना। शक्ति शिव की अर्धाङ्गिनी है और इसी दृष्टि से वह अर्धनारीश्वर है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शक्ति ही वाक् है, जिसे यहां प्राणानाम् उत्तमा ज्योतिः कहा जा चुका है।
प्रजापति और वाक्
दूसरे शब्दों में, महत् अथवा सलिलं से होने वाली उक्त अष्टाचक्र एकनेमि वाली सृष्टि वस्तुतः इसी वाक् का एक से अनेक होना है। इसी बात को निम्नलिखित ब्राह्मण वचनों में इस प्रकार कहा गया है --
(१) प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीन् नान्यं द्वितीयं पश्यमानस्तस्य वागेव स्वमासीद् वाग् द्वितीया स ऐक्षत हन्तेमां वाचं विसृजे। इयं वावेदं विसृष्टा सर्व विभवन्त्य एष्यतीति। जैब्रा २,२४४, तु. तां २०, १४, २
(२) प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग् द्वितीयासीत् तां मिथुनं समभवत् सा गर्भमधत्त, सास्माद् (प्रजापतेः) अपाक्रामत् सेमाः प्रजा असृजत्, सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्। काठ १२, ५, २७,१,१ क ४२,१ ।
इन दोनों उद्धरणों के आधार पर सृष्टि का मुख्य कार्य वाक् पर अवलम्बित है, वही गर्भाधारण करके नानारूपात्मक सृष्टि करती है। यह वाक् प्रजापति की ‘स्वं‘ है, जो सृष्टि करके पुनः उसमें प्रविष्ट हो जाती है। ‘प्राणानां वागुत्तमा‘ की उक्ति के साथ ही यह भी कहना उचित है कि वाक् रूप प्राण ही प्रजा बन जाता है। अतः प्राण से ही प्रजाओं की उत्पत्ति मानी गई है -- प्राणात् प्रजाः प्रजायन्ते मैसं ४, ७, ४)। इसलिए अथर्ववेदीय प्राणसूक्त में प्राण ही प्रजापति है -- ‘प्राणमाहुः प्रजापतिं‘। और प्राण ही प्रजा को इस प्रकार अनुवासित किए हुए है, जिस प्रकार पिता पुत्र को करता है –
प्राणः प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्।
प्राणो ह सर्वेस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ।। अथर्व ११,४,१०
प्राणरूप आपः की सृष्टि और काष्ठाएँ
अतः वाक् से होने वाली सृष्टि को प्राणरूप आपः की सृष्टि कह सकते हैं। सामान्यतः इस सृष्टि को व्यष्टिगत सृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें सक्रिय भूमिका सप्त आपः की रहती है। इस बात को यजुर्वेद में निम्नलिखित मन्त्र में उपस्थित किया गया है।
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्।
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ।।- वा,सं. ३४.५५
इस मन्त्र में सप्त प्राण रूपी ऋषियों[10] को तीन प्रकार से बताया गया है-
(१) शरीर में स्थित सात स्थूलप्राण -- दो चक्षु, दो श्रोत्र, दो नासिकारन्ध्र और एक मुख।
(२) अप्रमाद भाव से निरन्तर रक्षा करने वाले सात सूक्ष्म प्राण -- अर्थात्-अहंकार, मन और पंच ज्ञानेन्द्रियां।
(३) सुषुप्तिलोक में व्याप्त रहने वाले आपः नामक सात अति सूक्ष्म प्राण।
और इनके अतिरिक्त दो प्रसिद्धदेव, जिनको क्रमशः मूलप्रकृति और महत् कहा जा सकता है। इनमें से मूलप्रकृति को वह एकनेमि कह सकते हैं जिसके अन्तर्गत सप्त आपः और महत् से निर्मित अष्टाचक्र प्रवर्तित होता हुआ पहले बताया गया है। इन आपः को सप्त आपः कहने के साथ ही इनके लिए महतीः[11] और महीः[12] विशेषण भी प्रयुक्त हैं और इन्हें प्रथमजाः भी कहा गया है[13] आपः को सप्त, महतीः और महीः तथा प्रथमजाः कहने का क्या रहस्य है, उसका एक संकेत तो पूर्वोक्त यजुर्वेदीय मन्त्र से मिल गया है, परन्तु प्रतीकवादी आवरण को हटाकर इसे जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए हम कठोपनिषद् के निम्न उद्धरण की सहायता ले सकते हैं:-
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान् परः।। १,३,१०
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः।
पुरुषान् न परः किंचित् सा काष्ठा सा परा गति।। १.३.११
यहां आत्मा के व्यक्त और अव्यक्त स्तरों को काष्ठा कहा गया है। यह शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है[14] । कठोपनिषद में पराकाष्ठा का नाम पुरुष बताया गया है। इसी को ऋग्वेद ने अजन्मा, अस्रष्टा, असु आत्मा माना है[15]। यह अजन्मा से जायमान होने में स्थिति (अगतिमय प्रकृति) को त्याग कर विकृति को ग्रहण करता है। मूल प्रकृति उसकी अव्यक्त रहने की स्थिति है। अतः यहां पुरुष और अव्यक्त नाम से जो सांख्यमत के समान दो अलग-अलग सी काष्ठाएं लगती हैं, वे वस्तुतः एक ही काष्ठा के अन्तर्गत शक्तिमान (आत्मा) और उसकी शक्ति (प्रकृति) की अद्वैत और अव्यक्त इकाई को ही सूचित करती हैं। इस अद्वैत इकाई में अन्तर्निहित शक्ति का जब स्फुरण होता है, तभी अव्यक्त का व्यक्तीकरण आरम्भ होता है अथवा वेद के शब्दों में अजन्मा जायमान होता है। सांख्य दर्शन की शब्दावली में, तभी प्रकृति (अव्यक्त) में क्षोभ होता है और उसके फलस्वरूप महत् नामक बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी व्यक्तीकरण के स्तर को कठोपनिषद् ने आत्मा महान् कहा है। यह स्तर अव्यक्त स्तर से इसी बात में भिन्न है कि पहले जो शक्ति आत्मा में अन्तर्निहित थी, वह अब स्फुरित होकर बृहदारण्यकोपनिषद्[16] की भाषा में, अन्यदिव हो गई। इसी का नाम महत् है। इससे युक्त होने के कारण, अव्यक्त काष्ठा का पुरुष, अब महत् के योग से अगली काष्ठा में आत्मा महान् कहा जाता है। पुरुष की अव्यक्त मूल प्रकृति की पहली विकृति यह महत् है, जो बुद्धि, मन और अर्थ नामक अन्य विकृतियों में रुपान्तरित होती है। ये सभी, मनुष्य की सूक्ष्मस्तरीय व्यक्तित्व की काष्ठाएं हैं।
इसमें से बुद्धि को अहंबुद्धि कह सकते हैं, जो महत् नामक बुद्धि से भिन्न है। महत् अहंपूर्व बुद्धि है, जिससे युक्त होने से पुरुष की महान् संज्ञा होती है और उसे बुद्धि (अहंबुद्धि) से परे बताया जाता है। अहंबुद्धि से मन और मन से अर्थ उत्पन्न होते हैं। अर्थ से तात्पर्य मन से उद्भूत उन शक्तियों से है, जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श नामक पांच तत्वों को ग्रहण करती हैं। इन पाँचों अर्थों के साथ मन और अहंबुद्धि मिलाने से सात काष्ठाएं बनती हैं। ये प्रथम विकृति, महत् की विकृतियां है। ये ही महान् आत्मा और महत् (अहंपूर्व बुद्धि) के सात पुत्र हैं, जिन्हें नाराः वा नरसूनवः कहा जा सकता है। ये ही नर का पूर्व अयन हैं, क्योंकि उसके पूर्व यह असीम है, महान् है, अव्यक्त है, जबकि उक्त सप्त काष्ठाओं में उसे सीमित, लघु (रघु) और व्यक्त कहा जाता है। फिर भी, यह सूक्ष्म व्यक्त स्तर उसका पहला ही घेरा है, अतः पूर्व अयन कहा जाना ठीक है। दूसरा घेरा तो स्थूल इन्द्रिय स्तर पर बनता है, जिसे नव्य अयन कह सकते हैं। इसके सन्दर्भ में आत्मा की नर संज्ञा है। इस स्तर के अयन को वेद में प्रायः नर्य रथ[17] कहा जाता है, जबकि पूर्व अयन की पूर्वरथ[18] संज्ञा भी है।
प्रत्येक स्तर के इन सात प्राणों का उद्भव जिस अष्टम प्राण से होता है, उसी को सांख्य दर्शन में अष्टमी प्रकृति अथवा महत् कहा जाता है। वेद में आपः के साथ महत् शब्द का प्रयोग इस दृष्टि से विचारणीय है, क्योंकि महत् शब्द कठोपनिषद् के उक्त उद्धरण में नीचे की काष्ठाओं का स्रोत है। महतीः (ऋ ८.७, २२)[19] वा महीः (ऋ ६.५७, ४)[20] विशेषणों का प्रयोग आपः के साथ इसलिए सार्थक लगता है कि स्वयं महत् शब्द वेद में वही (कठोपनिषद् वाला) अर्थ रखता प्रतीत होता है। अव्यक्त आत्मा की जिस प्रकार प्रथम अभिव्यक्ति महत् है, उसी प्रकार महत् इन्द्र का प्रथम वीर्य है[21] । महत् वह नाम भी है जहां सभी देव इन्द्र में समाहित होते हैं और संभवतः इसीलिए वह देवों का एकमात्र अक्षर असुरत्व है, जो रहस्यपूर्ण गोपद[22] में जन्मता है। सविता महान् का वरणीय महत् छर्दि[23] कठोपनिषद् के आत्मा महान में सम्बन्धित महत् का याद दिलाता है, तो आपः और सूर्य में स्थित महत् नामक धन[24] सब देवों का महत् नामक अव[25] अथवा महत् नामक अपां गर्भः, जो देवों का वरण करता है[26], निस्सन्देह शब्द के औपनिषदक अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसलिए महत् को इन्दु का वह गुह्य नाम बताया जाता है, जो भूत और भव्य सभी का (ऋ १.५५, २) जन्मदाता है। इन्द्र का यह महत् जिस महती की उपज है, वह प्रथमा उषा है[27], जो अन्यत्र सत्या कहाती है। यह महती, सांख्य की उस अव्यक्त प्रकृति के समान है, जिससे प्रादुर्भूत होकर महत् बुद्धि अहंकार, मन तथा अन्य सभी तत्वों को जन्म देती है।
महत् शब्द के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वेद में महत् आपः का गर्भ और उक्त सप्त काष्ठाओं का तथा उनसे उद्भूत सम्पूर्ण सृष्टि का स्रोत है। इसके अतिरिक्त, महत् और इन्द्र का जो सम्बन्ध वेद में है, वही कठोपनिषद के महत् और आत्मा का है। यह सम्बन्ध विशेष महत्व का है, क्योंकि उपनिषदों के अनुसार इन्दु शब्द का अर्थ आत्मा ही है। ऐतरेयोपनिषद (१.१४)[28] इसीलिए आत्मा को इन्द्र कहने का औचित्य सिद्ध करते हुए एक व्युत्पत्ति देती है और फिर आज्ञान, क्रतु, जूति, दृष्टि धृति, मति, मनीषा, मेधा, विज्ञान, संकल्प, संज्ञान, स्मृति आदि नामों से अभिहित आत्मा को एष इन्द्र (३, २)[29] कहती है। इसी उपनिषद् ने आरभ्भ में ही स्वयं आपः की दृष्टि भी आत्मा से बताई है। अतः स्पष्ट है कि वैदिक आपः आध्यात्मिक शक्तियां हैं, न कि जल।
आपो देवीः बुद्धियां
इस प्रसंग में सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि वैदिक आपः बहुवचन तो है ही, साथ ही उन्हें सप्त आपः वा सप्त सिन्धवः कहकर उक्त सप्त काष्ठाओं की तुलना में भी बैठाया जा सकता है। दूसरे ये सप्त आपः प्रथमजा हैं और इन प्रथमों (प्रथमान् ऋ १०.१७, ११)[30] को जो द्रप्स जन्म देता है, उसी को आपः की प्रथम इन्द्रपान ऊर्मि[31] कहा गया प्रतीत होता है, जिसे इड पैदा करता है। इड की शक्ति को ही वेद में बुद्धिवाचक इडा से अभिहित किया जाता है। यह शक्ति ही इड का वह सहस्रार्ध भाग है[32], जो द्रप्स में परिणत होकर और सप्त आपः को जन्म देकर सप्त होत्राः को संभव बनाता है[33]। एतएव यह स्पष्ट है कि इडा नामक बुद्धि से उत्पन्न ये सप्त आपः भी वे ही सात बुद्धियां अथवा आध्यात्मिक शक्तियां है, जिन्हें पहले काष्ठाएं कहा गया है।
इस सन्दर्भ में, यह भी उल्लेखनीय है कि इड और इडा उसी प्रकार एक दूसरे से सम्बद्ध है जैसे उपनिषद् का महान् (आत्मा) और महत् (बुद्धि)। इड जिस प्रकार अग्नि प्रथमः है[34], जो पद में प्रज्वलित है, उसी प्रकार इडा भी समिद्ध प्रज्वलित होती कही जाती है[35], क्योंकि वस्तुतः बुद्धि (धी) द्वारा अग्नि को वरेण्य बनाया जाना अथवा इडा द्वारा इस वरेण्य को धारण किया जाना[36] ही इड(अग्नि) और इडा का समान रूप से समिद्ध होना कहलाता है। जिस पद में अग्नि जलता है, वही इडा का पद (इडायास्पद) है, जिससे सम्बद्ध आत्मा रूप इड को भी जातवेदाः[37] वा प्रथम अग्नि इड[38] कहा जाता है।
इड और इडा का यह संयुक्त पद ही वह सलिल है[39], जिसके मध्य से सप्त आपः देवीः का उद्गम है। इसीलिए उसी सलिल को आपः का गर्भ कहा जाता है। सलिल से उत्पन्न वत्सद्वय (वत्सौ)[40] यही इड और इडा अर्थात् महान् आत्मा और महत् है। इडा अथवा महत् वह माया (अहंपूर्व बुद्धि) है, जिससे बृहती नामक दूसरी माया (अहंबुद्धि) उपजती है[41]। बृहती (अहंबुद्धि) षष्ठ बृहत् (मन) को जन्म देती है, जिससे पांच साम (अर्थ) उत्पन्न होते हैं[42]। सलिल को ही गतिशील ब्रह्म (ब्रह्मैनत) कहा जाता है, जिसमें इड और इडा दोनों एक दूसरे से संयुक्त रहते है, इस बात को विपश्चित ही जान पाते हैं।[43]
अहंबुद्धि युक्त आत्मा का नाम कश्यप है। यह उक्त छह बृहतों (मन तथा पांच अर्थ) से युक्त आत्मा के ऋषयः कहे जाने वाले रूपों में युक्त और योग्य कहा जाता है।[44] आत्मा के कश्यप रूप के लिए परिभाषिक शब्द जीव है। कश्यप नाम की सार्थकता इसी में है कि कशा (अहंपूर्वबुद्धि-इडा) द्वारा कश्य जो हिरण्य वा मधु (ऋ ८, ३३, ११, १, २२, ३) है, उसका पालन करे और पान करे। पर यह संभव तभी है, जब उसकी अहंबुद्धि के द्वारा सभी छह बृहतों की काष्ठाओं में अहंपूर्व बुद्धि (इडा, महत्) की धारा प्रवाहित होती रहे। इन छह बृहतों के सन्दर्भ में जीव के जो छह रूप बनते हैं, उनके साथ कश्यप को लेकर इन सातों से सप्तऋषियों और सप्त अदिति-पुत्रों की तुलना भी संभव है।
सप्त काष्ठाओं में निहित दीर्घतमः और अष्टम काष्ठा :-
दुःख की बात यह है कि हमारा कश्यप (जीव) जिस अहंबुद्धि से युक्त है, वह ऐसी उषा वा सरस्वती है जिसके ऋत और अनृत नाम से दो द्वार हैं,[45] । एक अवृक् और दूसरा वृक् (भेड़िया) से युक्त। इसी दृष्टि से, उषारात्री वा उषानक्ता नाम से एक संयुक्त काष्ठा की कल्पना वेद में की गई है और ब्राह्मणग्रन्थों और पुराणों में विनता एंव कद्रू नाम से कश्यप की दो पत्नियां क्रमशः देवरूप गरुड़ों और दैत्य रूप अहियों की माता कहलायी। वेद में विनता को अदिति के उस रूप में देखा जा सकता है, जो अपने सप्त पुत्रों से युक्त है[46] और कद्रू को उस प्रथमजा के रूप में जो वृत्र (अहि) की माता और अहियों में प्रथमजा है[47] । वृत्रमाता से उत्पन्न प्रमुख वृत्र वा अहि दीर्घतमः (अज्ञानान्धकार) है, जो अस्थिर और चंचल काष्ठाओं में मध्य निहित होता है[48]। पर अनेक वृत्रों अथवा अहियों का जो उल्लेख प्रायः देखने को मिलता है, उसका अभिप्राय यही है कि अनेक काष्ठाओं में विभक्त होने से एक ही अज्ञान्धकार वृत्रों अथवा अहियों के रूप में माना जाता है। इसलिए काष्ठाओं को[49] मुक्त करने के लिए अमित्रों को नष्ट करने की जिस प्रकार प्रार्थना की जाती है, उसी प्रकार दस्यु शम्बर के भेदन से सभी काष्ठाओं[50] को हिलाने की बात कही जाती है अथवा सभी काष्ठाओं और वृत्रों में इन्द्र को आने के लिए आहूत किया जाता है[51]।
इस अनेक काष्ठाओं के अतिरिक्त भी एक काष्ठा है, जिसके सुषुप्त वृषभ इन्द्र का युञ्ज[52] उस व्यक्ति द्वारा द्रष्टव्य वा ज्ञातव्य है, जो अन्य काष्ठाओं में कैद गायों को जीतना चाहता है। वृषभ के इस युञ्ज में ही इस काष्ठा की प्रगति है, जिसे अपनी बुद्धियों के द्वारा खोजते हुए (धीर्भिः विप्राः प्रमतिमिच्छमानाः)[53] इन्द्राग्नी का आहवान करते है। अन्य काष्ठाओं में जब असत्य (दीर्घतमः) की मति हो, तो उसको नष्ट करने वाली सत् की मति वा सन्मति (सतः मतिम्) इसी काष्ठा में से पैदा करनी होगी[54], क्योंकि जहां अन्य काष्ठाएं सीमित हैं, वहीं यह उर्वी काष्ठा है, जिसमें उक्त प्रमति वा सन्मति के रूप में धन छिपा है (हितं धनम्)[55] जो आत्मा के तुरीय नामक यज्ञिय रूप के साक्षात्कार में भी सहायक होता है[56], इसलिए स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि यह उर्वी काष्ठा वही सलिल पद है, जहां इड और इडा (अहंपूर्व बुद्धि वा महत्) दो परस्पर संयुक्त वत्सों के रूप में कल्पित किये गये थे और अन्य काष्ठाएं वे सप्त पद है, जिन्हें अहंबुद्धि, मन और पांच अर्थ और सलिल से उत्पन्न होने वाले सप्त आपः वा सप्त सिन्धवः की काष्ठाएं माना गया है। इन सातों के सन्दर्भ में जीवात्मा को भी सप्त रूपों में कल्पित किया जाता है।
आपः का सलिल और अष्टपुत्रा अदिति
इसका तात्पर्य यह है कि जिस सलिल के मध्य से सप्त आपः आते है और जहां से असत् को नष्ट करने के लिए प्रमति, सन्मति अथवा इन्द्र आता है, वह मनुष्य के व्यक्तित्व की अष्टम काष्ठा है। इसलिए इन आठ काष्ठाओं के सन्दर्भ में जीवात्मा के आठ रूपों की कल्पना की गई है। ये ही अदिति के आठ पुत्र हैं, जिनमें से सप्त आपः के समान सात पुत्र तो एक साथ बताये जाते है और आठवां पुत्र मार्ताण्ड विशिष्ट है[57]। सात पुत्रों के द्वारा तो अदिति देवों (बहुवचन) तक पहुचती है, पर मार्ताण्ड को परा ग्रहण करती है और प्रजा के पालन तथा मृत्यु के निवारण के लिए उसी को पुनः सप्तपुत्रों के पूर्व्य युग[58] में ले जाती है, जो निस्सन्देह, सप्त आपः का क्षेत्र है। अतः इस मार्ताण्ड की तुलना मिस्र के उस सुनहरे अंडे से की जा सकती है, जो मार्ताण्ड के समान आपः (जलों) पर प्रकट होता है। यही वह सूर्य के समान तेज वाला अण्डा है, जो मनुस्मृति के अनुसार आपः में उद्भूत हुआ और वेद में वर्णित यही वह गर्भ कहा जा सकता है, जिसे धारण करती हुई आपः अग्नि को जन्म देती है[59] अथवा वह दक्ष है, जिसे धारण करती हुई वे यज्ञ को जन्म देती हैं[60] क्योंकि सप्त आपः का क्षेत्र ही नानात्वमयी सृष्टि का क्षेत्र प्रतीत होता है। इसीलिए उक्त अग्नि का जन्म लेकर, सब देवों का एक असु (देवानां समर्वतासुरेकः) और यज्ञरूप में सब देवों में एक अघिदेव (देवप्वधि देव एक आसीत्) होता बताया गया है। अथर्ववेद (८, ९, १७-१८) इसी दृष्टि से, यज्ञरूप नानात्वमयी सृष्टि के अन्तर्गत, विभिन्न प्रतीकों द्वारा सप्तविध सृष्टि का वर्णन करता हुआ सप्त सुपर्णो, सप्त छन्दों, सप्त दीक्षाओं, सप्त होमों, सप्त समिधाओं, सप्त ऋतुओं और सप्त आज्यों का उल्लेख करता है। इन सभी प्रतीकों की व्याख्या करना यहां विषयान्तर होगा। पर इतना तो स्पष्ट है कि ये सभी सप्तक उक्त सप्त काष्ठाओं के सन्दर्भ में समझे जाने चाहिएं। आठवीं काष्ठा इन सबका गर्भ वा अंडा प्रस्तुत करती है, जिसके कारण कुल सृष्टि अष्टविध हो जाती है।
इसी दृष्टि से अष्टभूत हैं, जो प्रथमजा ऋतस्य माने गये हैं और दिव्य ऋत्विजों की संख्या भी आठ है[61]। इस सब अष्टविध सृष्टि की जननी अदिति को अष्टयोनी, अष्टपुत्रा तथा अष्टमी रात्रि[62] कहा जाता है। अदिति की इस अष्टविध सृष्टि में से सभी आठों का सम्बन्ध इन्द्र से (अष्टेन्द्रस्य) है, सातों का सप्त ऋषियों से (ऋषीणां सप्त सप्तधा) तथा छह का यम से (षड् यमस्य)[63] । पर अदिति का एक केवली रूप भी है, जो इन्द्र के लिए प्रथम पीयूष दुहाने वाली सृष्टि[64] कही जाती है। इस प्रथम पीयूष की तुलना पूर्वोक्त आपः की प्रथम इन्द्रपान ऊर्मि (ऋ ७.४७, १)[65] से भी की जा सकती है, जो निस्सन्देह पवमान सोम है[66], जिसको आपः की रचना करने वाला तो बताया जाता ही है[67], पर जो मतियों, अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु का भी जनक है[68] और जायमान पूर्व्य और अद्रि में आपः के भीतर दुहा जाने वाला है।[69]
इस विवेचन से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते है। पहला तो यह कि अदिति के सप्तपुत्रा और अष्टपुत्रा रूप ऊपर देखे गये, उनके अतिरिक्त एक तीसरा केवली रूप भी है, जो इन्द्र के लिए सोम दुहता है। दूसरा यह कि यह सोम इन्द्र को मिलता है अष्टम काष्ठा में, जहां वह (सोम) इन्द्र के अतिरिक्त अग्नि, सूर्य, विष्णु आदि को भी पैदा करता है और कि इस सोम की पहुंच सप्त आपः के क्षेत्र तक है। यह एक विचित्र बात लग सकती है। पर वेद में इस बात को युक्तिसंगत बनाने के लिए अदिति (जिसका अर्थ है अखण्ड) को नवगज्जनित्री[70] नाम दिया है और उसमें बड़ी महिमाएं छिपी हुई (महान्तः महिमानः) मानी हैं। नवगज्जनित्री का अर्थ यही हो सकता है कि वह नौ काष्ठाओं में विद्यमान होती हुई अष्टकाष्ठाओं की जननी भी है, इसलिए जो बड़ी महिमाएं इसके अन्दर छिपी हुई बताई गई हैं, वे अष्ट काष्ठाओं में प्रकट होने वाली शक्तियां हैं। पर वह जनित्री बनती है अष्टम काष्ठा में, क्योंकि प्रथम पीयूष और इन्द्रपान कही जाने वाली आपः की प्रथम ऊर्मि (सोम) आदि का जन्म भी वहीं होता है। अतः नवगज्जनित्री अदिति केवली वह अव्यक्त तत्व है, जिसे उपनिषद् के उद्धरण की व्याख्या करते हुए, अजन्मा परा काष्ठा (पुरुष) में अन्तर्निहित माना गया है। इसलिए अष्टविध सृष्टि की जनित्री होती हुई भी, वह अजन्मा काष्ठा सहित नव काष्ठाओं में विद्यमान मानी गयी है। अष्टम काष्ठा में होने वाली इसकी अभिव्यक्ति को प्रथम उषा वा एकाष्टका कहा गया है, जो अपने से नीची सात काष्ठाओं में उसी प्रकार प्रविष्ट मानी गई है[71], जिस प्रकार नवगज्जनित्री। इस प्रकार प्रत्येक काष्ठा अपने से नीची अन्य सभी काष्ठाओं में प्रविष्ट है।
नवगज्जनित्री का नाम विराट गाय है, जिसके स्थित (उपतिष्ठमाना) होने से यज्ञ (सृष्टि) रुक जाते हैं और जिसके गतिशील (प्रच्युता) होने पर चल पड़ते हैं और जिसके प्रसवव्रत में यक्ष (पुरुष आत्मा) गतिशील हो जाता है -
यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त, उपतिष्ठन्त उपतिष्ठ मानाम्।
यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति, सा विराड् ऋषयः परमे व्योमन्।। अथर्व ८, ९, ८
यह प्रसवव्रत वस्तुतः अष्टम काष्ठा के रूप में अव्यक्त प्रकृति का होना है। यही सलिल अवस्था है, जहां इसके वत्स इड और इडा उत्पन्न होते हैं। और यही अग्नि, यज्ञ, आपः, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का गर्भ है। यह अष्टम काष्ठा आत्मा की जायमान अवस्था है, जिसमें वह गर्भ में स्थित होता हुआ कहा जाता है। इसका प्रतीकात्मक चित्रण ऋ ४.१८, ४.२६, ४.२७ में मिलता है। वहां अपने लिए अहं (मैं) का प्रयोग करने वाला आत्मा है[72]। वह दृष्टिभेद से वामदेव का श्येन भी कहा जाता है। ऐतेरेयोपनिषद् (३, १-३) के अनुसार वह इन्द्र, ब्रह्म, असु, प्रजापति भी कहाता है। गर्भस्थित हुआ वह सभी देवों के जन्मों को जानता है[73], सब देव वस्तुतः इस महान् आत्मा की विभूतियां[74] ही हैं। यही अस्रष्टा आत्मा वह प्रथम जायमान रूप और वत्स है[75] जिस पर नीचे के सप्त काष्ठाओं की नानात्वमयी सृष्टि के वे सप्ततन्तु (अहंबुद्धि, मन और पांच अर्थ) प्रसारित किए जाते है, जिन्हें सप्त आपः आदि कहा जाता है।
एक दूसरी दृष्टि से, सप्ततन्तु की सृष्टि को सौ तन्तुओं की सृष्टि भी माना जाता है। यह एक सौ एक देवकर्मों द्वारा प्रसारित यज्ञ है[76] जिसके तन्तुओं को फैलाने वाला और समेटने वाला एकमात्र पुरुष (आत्मा) है। इन देवकर्मों के समानान्तर अहि (वृत्र वा शंबर) के भी सौ पुर हैं, जो गर्भावस्था में महान् आत्मा को घेरे हुए हैं। ये ही वे सौ पुर हैं, जो आत्मा को, मर्त्य आर्य (सप्ततन्तु क्षेत्रीय जीवात्मा) के लिए आपः लाने में, और सभी देवों वाली सर्वताता यज्ञसृष्टि को फैलाने में[77] नष्ट करने पड़ते है। ये पुर जब केवल सप्त तन्तुओं वा सप्त आपः को घेरने वाले माने जाते है, तो उनकी संख्या केवल सात होती है[78] और सात ही माने जाते है अहि वा दानु[79] । इससे स्पष्ट है कि सौ देवकर्मों और सौ दैत्यकर्मों की द्विधा सृष्टि वस्तुतः आत्मा की उन सप्त काष्ठाओं के अन्तर्गत होती है, जिन्हें अहंबुद्धि, मन और पांच अर्थो के रूप में स्वीकार किया जाता है। आत्मा का यही रूप मर्त्य वा जीव है, जो अहंबुद्धि के दूषित प्रभाव से अपने उस महान् स्वरूप को भूल जाता है, जो अष्टम काष्ठा में है और जो उसका उद्गम है।
सिन्धु और सप्त आपः
अतः सप्त तन्तुओं वा सप्त सिन्धुओं (आपः) के स्तर की जो जीवकेन्द्रित नानात्वमयी सृष्टि प्रतीत होती है, वह अष्टम काष्ठा के बिना नहीं सोची जा सकती है। नवगज्जनित्री कही जाने वाली स्वयंभू अदिति सर्वप्रथम अष्टम काष्ठा में ही गर्भधारण करती है। अतः यह अष्टम काष्ठा का गर्भ ही वस्तुतः आद्यासृष्टि है। इसी का नाम सिन्धु है जिसे सप्त सिन्धवः(आपः) द्वारा पार करके इन्द्र (महान् आत्मा) निन्यानवे नदियों[80] की सृष्टि तक पहुंचता है और मनुष्यों और देवों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सिन्धु को लेकर इन नदियों की संख्या सौ होती है, जिनकी तुलना सौ देवकर्मों के यज्ञ से की जा सकती है। इस प्रकार सिन्धुओं को शतरूपा सर्वताति यज्ञ के रूप में प्रकट होने वाली भी माना जा सकता है। यह सिन्धु मातृतमा है[81], जबकि सप्त सिन्धवः वा सप्त आपः केवल माताएं हैं[82] । सिन्धु वह समान योग है, जहां सप्त आपः का रथ अन्ततोगत्वा पहुंचता है। सिन्धु हिरण्यवर्तनि है[83] और उसका गर्भ (महान् आत्मा) हिरण्यगर्भ कहलाता है। इसी गर्भ को लेती हुई सप्त आपः सिन्धु से बाहर आती है और अग्नि को सब देवों के असुरूप में वा देवाधिदेव यज्ञ-रूप में जन्म देती है। अतः सप्त आपः एक बार तो सिन्धु रूप में और दूसरी बार सप्त सिन्धुओं के रूप में जन्मती है। अतः आपः को द्विजा (दो बार जन्म लेने वाली) और प्रथमजा (प्रथम बार जन्म लेने वाली) दोनों ही विशेषण दिये जाते हैं[84]। प्रथमजा कहने पर आठों काष्ठाओं की आपः (अष्ट जाताः प्रथमजाः ऋतस्य)[85] का बोध होता है, तो द्विजा कहने से केवल नीचे की सप्त काष्ठाओं की आपः का। इस प्रकार अष्टपुत्रा और सप्तपुत्रा अदिति के समान सिन्धु भी अष्टरूपा और सप्तरूपा दोनों ही कही जा सकती है और तीसरा उसका सर्वताति यज्ञसृष्टि का रूप है।
इस सिन्धु के तीनों रुपों का वर्णन विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से वेदों में प्राप्त र्है। केवल अष्टम काष्टा की दृष्टि से वह दैव्य अष्टमविश्व है[86], जिसमें स्थित महान् अष्टम शूर, चेतनपिता और यज्ञसृष्टि[87] का नेता कहा जाता है। सप्त सिन्धुओं का उद्गम होने से इसे सप्तबुध्नअर्णव (सप्त आपः का बुध्न पैंदा) कहते हैं।[88] यह अर्णव सप्त सिन्धुओं के रूप में मर्त्यस्तर की सृष्टि में पहुंचता है और सर्वताति का रूप ग्रहण करता है। इन्हीं तीनों रूपों के संदर्भ में आत्मा को सूक्ष्म और स्थूल काष्ठाओं के भेद से दो रूपों में चित्रित किया गया है। सिन्धु और सप्त सिन्धुओं की सृष्टि में भी प्रथम के साथ वह मनुपिता और प्रमति (इडा वा महत्) के मिथुनत्व का युञ्ज रूप यज्ञ[89] (ऋ १०.१००, ५)[90] है, जबकि वह दूसरे स्तर पर समिद्ध मनुष् है, देवों का यजन करने वाला जातवेदाः है[91], तो तीसरे स्तर पर वह अनेक मानुषों के रूप में माना जाता है। द्वितीय और तृतीय स्तर पर सृष्टि को क्रमशः ऋषियों और मानुषों का यज्ञ कहा जाता है[92], जिनमें सप्त सूक्ष्म काष्ठाओं के सन्दर्भ में कल्पित सप्त मानुष नामक अग्नि सभी सिन्धुओं में (विश्वेषु सिन्धुषु) स्थित[93] कहा जाता है।
विश्वेषु सिन्धुषु के सन्दर्भ में, सिन्धु का एक सुन्दर चित्र ऋ १०, ७५ में उपलब्ध है। यहां सिन्धु को अन्य सिन्धुओं (आपः) का उत्तम महिमा कहा गया है, क्योंकि वह अपने ओज द्वारा उन सब आपः से श्रेष्ठ है, जो सात-सात के तीन वर्षों में (सप्त-सप्त त्रैधा) गतिशील (ऋक्।) अन्य आपः वस्तुतः वे मार्ग हैं, जो वरुण ने सिन्धु के लिए अपने बलों (वाजान्) को दौड़ने के लिए (ऋक् २) बनाएं हैं। सिन्धु वृषभ हंै। सिन्धु वृषभ है, जो न मार्गी पर चलते समय अनन्त बल, शब्द और वृष्टि करता हुआ (ऋक ३) चलता है। पर यह गमन केवल एक तरफा नहीं है, क्योंकि सभी आपः भी सिन्धु के पास ऐसे आते हैं, जैसे माताएं वा गायें अपने शिशु के पास (ऋक् ४) आती हैं। इसका अभिप्राय आध्यत्मिक दृष्टि से यही है कि मनुष्य व्यक्तित्व की उपर्युक्त अष्ट काष्ठाओं में से अतिमानसिक सिन्धु मनोमय, प्राणमय और अन्नमय स्तरों की सप्त-सप्त त्रेधा आपः की शक्ति का स्रोत भी है और उनके प्रवाहों का पुनर्ग्रहीता भी। इन इक्कीस शक्तिप्रवाहों का स्वास्थ्य, नवीनीकरण के अभाव में संकटापन्न हो जाये, यदि वे पुनः अतिमानसिक सिन्धु में पहुंचकर दीर्घतमः (वृत्र) से उत्पन्न दुरित को दूर न करे लें।
सिन्धुमाता सरस्वती :
जैसा कि पहले कहा गया है, सिन्धुकाष्ठा का एक युञ्ज है, जिसमें नवगज्जनित्री विराट् गाय के दोनों वत्स(बछड़ा और बछिया) परस्पर संयुक्त हैं।[94] अतः वृषभ का युञ्ज होने से यदि उसे पुल्लिंग वृषभ कहा जा सकता है, तो धेनु का युञ्ज होने से उसे स्त्रीलिंग (युवती)[95] भी कहा जा सकता है। एक दूसरी कल्पना के अनुसार, इस काष्ठा का युञ्ज वस्तुतः इन्द्र के दोनों अश्वों का युञ्ज है[96], जिनमें से एक पुल्लिंग तो दूसरा स्त्रीलिंग है। अतः सिन्धु युवती को घोड़ी के समान दर्शनीय भी कहा जाता है।[97] दूसरे शब्दों में, सिन्धु नामक अतिमानसिक काष्ठा में इड और इडा वृषभ और धेनु, महान् आत्मा और महत् दोनों की संयुक्त इकाई है।
यह संयुक्त इकाई जब सप्त सिन्धुओं के माध्यम से सभी सिन्धुओं में (विशेष सिन्धुषु) परिणत होकर सर्वतति सृष्टि का रूप ग्रहण करती है, तब यह अश्व और अश्वा, दोनों से युक्त, अश्विन् रथ द्वारा अपने वाज को अनेकशः विभक्त करती है।[98] दूसरे शब्दों में, अब इकाई द्वैत ग्रहण करके, अनेकता में परिणत होती है। इसी का अर्थ है वृषभ इन्द्र को दो अश्वों द्वारा यज्ञसृष्टि में ले जाया जाना, अथवा सिन्धु का सप्तविध होकर वा मनुष का सप्तमानुष होकर सभी सिन्धुओं में पहुंचना, अथवा सिन्धु माता का सप्तथी सरस्वती होना[99] और सभी कामना करने वाली और दुधारू सुन्दर धाराओं (आपः) का एक साथ पहुंचना। इस प्रकार, जो सिन्धु माता सरस्वती प्रथमा काष्ठा में एक आयसी पूः के रूप में स्थिर थी, वह प्रवाहित हो पड़ती है और अन्य सब आपः को अपनी महिमा से अभिभूत कर लेती है-
प्र क्षोदसा धायसा सस्र एषा, सरस्वती धरुणमायसी पूः।
प्रबाबधाना रथ्येव याति, विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः।। ऋ. ७.९५.१
इस प्रकार, यह सरस्वती समुद्र (प्रथम काष्ठा) से आने वाली, अनेक गिरियों (काष्ठाओं) के निमित्त जाने वाली और सभी नदियों (आपः) की एक इकाई (एका नदीनाम्) बन जाती है[100], जिससे वह महान् सिन्धु (महो अर्णः) सरस्वती अन्य काष्ठाओं की बुद्धियों को विविध रूप से प्रकाशित करने वाली, सुमतियों को प्रबुद्ध करने वाली और यज्ञसृष्टि को धारण करने वाली कही जाती है।[101]
ऋत के दो द्वार और वृत्रघ्नी सिन्धुमाता
सुमति को प्रबुद्ध करने की आवश्यकता दुर्मतियों के प्रकोप के कारण पड़ती है। पर इन द्विविध मतियों के उद्गम स्थान, ऋत के दो परस्पर विरोधी द्वार हैं। इनके नाम ऋत और अनृत हैं। इनको अन्यत्र द्युलोक के क्रमशः अवृक् और सवृक् द्वार कहा गया है। वृक् का अर्थ भेड़िया होता है और वृक वेद में वृत्र का प्रतीक है। अतः उषा से प्रार्थना की जाती है कि वह हमें अवृक द्वार प्रदान करे - प्र नो यच्छतादवृकं पृथु।[102] वृक एक अघ (अघो वृको)[103] है। अतः उस पथ को छोड़ना है[104] । अग्नि से उसको दूर करने की प्रार्थना है[105] , क्योंकि इसके नष्ट होने पर ही भद्र[106] संभव है। यह अघ एक दुःशंस और मर्त्य रिपु है। यह द्वैत का प्रेमी (द्वयु) है। अतः हमारे हृदयों में विद्यमान देवों को यह जानने की आवश्यकता है कि द्वैतप्रेमी (द्वयु) कौन है और अद्वैतप्रेमी (अद्वयु) कौन-सा है[107] ।
इस अघ रूपी वृत्र का विनाश तभी संभव है, जब प्रथमा काष्ठा सिन्धु अथवा प्रथमा उषा के उदय से सूर्यरश्मियों से प्रवाहित होने वाली उषाएं ज्योति को भरती हुई प्रकट हों। ये ही उषाएं सिन्धु माताएं हैं। इनसे सूर्य उषा और सोम के साथ, अभद्र अघ का नाश कर भद्र करने की प्रार्थना की गई है । यह प्रसंग में वेद यह स्पष्ट करना नहीं भूलता कि जिस प्रथमा उषा अथवा सिन्धु से अन्य उषाएं अथवा सिन्धवः अघनाशन में समर्थ होती हैं, वह वही बुद्धि (धिषणा) है, जिसे सविता का श्रेष्ठ वरेण्य भाग और स्वस्ति अग्नि[108] कहा जाता है और जो प्रसिद्ध गायत्री ऋक् का वरेण्यं[109] भर्गः है। इसी दृष्टि से सिन्धुमाता सरस्वती वृत्रघ्नी है और उसकी सहायक सप्त सिन्धवः के सन्दर्भ से, उसे सप्तस्वसा कहा जाता है। सभी काष्ठाओं की रक्षा करने वाली यही पहली काष्ठा है। इसलिए सरस्वती बुद्धियों की रक्षिका (धीनामवित्री) कहलाती है और बुद्धियों के अथवा अपने रूपान्तरों, सारस्वतों के साथ (सरस्वती सारस्वतेभिः)[110] याद की जाती है। ये सारस्वत और सिन्धुमाता सरस्वती के सिन्धवः एक ही हैं। अतः ‘सरस्वती सिन्धुभिः कथन सही अर्थ रखता है।
सिन्धु की त्रिविध बुद्धि :
यद्यपि इस प्रकार सिन्धुमाता सरस्वती के वर्णन से बुद्धि के सरस्वती पक्ष को अधिक महत्व मिल गया है, पर वस्तुतः सिन्धु के सरस्वती, इडा और भारती नाम से तीन पक्ष हैं। इन्हीं को तिस्रो देवीः[111] भी कहा जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सिन्धु का सलिल एक युञ्ज है, जिसमें महान् आत्मा और उसकी महद् बुद्धि एक संयुक्त इकाई के रूप में है। अतः इस इकाई को बुद्धि (धिषणा) और स्वस्ति अग्नि भी कहा जाता है और अग्नि को इसी आधार पर अदिति, भारती, इडा तथा सरस्वती के रूप में भी स्मरण किया जाता है-
त्मग्ने। अदितिर्देव। दाशुषे, त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा।
त्वामिडा शतहिमासि दक्षसे, त्वं वृत्रहा वसुपते! सरस्वती।। ऋ २.१, ११
अदिति अखण्ड और अव्याकृत रूप है। वह सरस्वती, इडा और भारती नाम से तीनों पक्षों में व्याकृत होती है। अदिति (महत्) को अरस्तु की शुद्ध बुद्धि और इस्लामी परम्परा की अल-अक्ल कह सकते हैं। मानव जीवन में यही बुद्धि क्रिया, ज्ञान और भावना की शक्तियों में प्रकट होती है। जैसा कि आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा, ये ही तीनों शक्तियां वेद में क्रमशः सरस्वती, इडा और भारती नाम से जानी गई हैं। यद्यपि निम्न स्तर पर ये तीनों अलग अलग देखी जा सकती हैं, पर अष्टम काष्ठा (सिन्धु) के स्तर पर वे उससे अभिन्न, उसके ही तीन पक्ष हैं, जिन्हें द्वारः कहा जाता है।
ये द्वारः (बहुवचन) हैं, जो अपनी महद् बुद्धियों (महद्भिः) द्वारा देव-रथ (जायमान महान् आत्मा) को धारण करती हैं[112] अथवा द्वारो देवीः हैं, जो अलंकृत स्त्रियों के समान अपने पतियों (आत्मा की विविध विभूतियों) के निमित विविध रूप ग्रहण करती हैं[113] , अथवा द्वारः है, जिन्हें इन्द्र ने अनन्त अश्म में छिपी निधि को बाहर निकालने के लिए खोला[114]। द्वारः देवीः के लिए प्रायः उर्विया, सुप्रायणा वा अजुर्या विशेषणों तथा विश्रयन्ताम् क्रिया का प्रयोग होता है[115] और वे देवों के लिए फैलाने वाली वा विविध रूप धारण करने वाली[116] हैं, यद्यपि वे मूलरूप में पवमान सोम से सुष्टुत और हिरण्यय[117] हैं। विविध रूप ग्रहण करने का अभिप्राय है अष्टम काष्ठा के हिरण्यय रूप को छोड़ कर नीचे की काष्ठाओं की नानात्वमयी यज्ञसृष्टि में परिणत होना । इसी बात को स्पष्ट करते हुए, सुन्दर रूप वाली तीन देवियों (सरस्वती, इडा और भारती) को पवमान की मही कहा गया है और उन्हें हमारे यज्ञ में आने के लिए आहूत किया गया है:-
भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही।
इमं नो यज्ञमागमन् तिस्रो देवीः सुपेशसः।। ऋ ९.५, ८
तीन द्वारों वा देवियों के रूप में कल्पित महद्बुद्धि के तीनों पक्षों के पृथक्-पृथक् स्वरूप की ओर भी संकेत मिलता है। इस दृष्टि से सरस्वती का सम्बन्ध कर्मवाचक अपस्[118] से विशेष महत्व रखता है। वह अपसामपस्तमा[119] अर्थात् कर्मों में सर्वाधिक क्रियाशील कही जाती है। अतः वह महद् बुद्धि के क्रियापक्ष की द्योतक प्रतीत होती है। भारती का विशेषण विश्वतूर्ति[120] भावनात्मक त्वरण का सूचक है। अतः भारती को महत् के भावना-पक्ष का प्रतीक माना गया प्रतीत होता है। भारती को वरूत्री (आवरण करने वाली) बुद्धि[121] कहना भावना के सम्मोहक पक्ष की ओर ही संकेत करता है। भावना निस्सन्देह मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ओतप्रोत करके क्षणभर में उसके क्रिया और ज्ञान को प्रभावित कर देती हैं सरस्वती और भारती से भिन्न स्वरूप इडा का है। इडा और इड का विशेष सम्बन्ध संज्ञान अर्थात् ज्ञानशक्ति से है। ज्ञानशक्ति को प्रायः अग्नि-रूप में कल्पित किया जाता है। तदनुसार इडा भी समिद्ध होती है और अग्नि के सुदीप्त वरेण्य रूप को धारण करती है। इडा को जब मनुष्यस्यशासनी कहा जाता है, तो भी इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य के ऊपर क्रिया अथवा भावना की अपेक्षा ज्ञानशक्ति का ही शासन होना चाहिए और होता है।
फिर भी, व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर, भावना और ज्ञान, दोनों में क्रिया का समावेश मिलेगा। अष्टम काष्ठ का महान् आत्मा जब अन्य काष्ठाओं के नानात्व में व्यक्त होता है, तो वह सब देवों में सर्वाधिक क्रियाशील (अपसामपस्तमः) उसी प्रकार कहा जाता है, जिस प्रकार महद् बुद्धि की प्रतीक सिन्धु के लिए अपसामपस्तमा विशेषण का प्रयोग होता है। सामान्य भाषा में भी, भावना करने और जानने को क्रिया के अन्तर्गत ही रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भावना और ज्ञान दोनों ही क्रियामूलक है। कम से क निचली सप्त काष्ठाओं के स्तर पर तो यह स्पष्ट ही है। हो नवम काष्ठा की बात दूसरी है, जहां नवगज्जनित्री अखण्डबुद्धि (अदिति) स्थिर हो जाने से सभी यज्ञकर्म रूक जाते हैं। जब अष्टम काष्ठा में उसका व्रतप्रसव आत्मा (यज्ञ) को सक्रिया करता है, तब से तो क्रिया और तन्मूलक भावना और ज्ञान का आरम्भ मानना ही पड़ेगा। अतः अष्टम काष्ठा (सिन्धु में महद् बुद्धि के तीनों पक्षों का उद्रेक स्वीकार करना होगा। पर वह अनेकत्व नहीं, एकत्व होगा। इसलिए इन तीनों को उससे भिन्न, द्वारः माना गया है। जैसे एक घर में तीन द्वार होने पर भी घर एक ही रहता है, वैसे ही भावना-ज्ञान-क्रिया का उद्भव होने पर भी अष्टम काष्ठा एक ही रहती है।
आपः शब्द का महत्व
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से आपः को जहां हमने ‘ओम् सत्यं’ में प्रतिष्ठित देखा, वहीं उसे महत् सलिल के मध्य से प्रवाहित होकर अनेक रूप ग्रहण करते पाया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ ‘प्राणो वा आपः अथवा ‘आपो वै प्राणाः’ की उक्ति बार-बार क्यों दोहराते हैं। मूलतः आपः उन दिव्य प्राणों का द्योतक हैं, जो अपने शुद्धतम रूप में महत् सलिलं अथवा सिन्धु में प्रकट होते हैं, यही महत् सलिलं अथवा सांख्य दर्शन में वह महत् बुद्धि कही गयी है, जो मूल प्रकृति से उद्भूत होकर अहंकार मन और सभी इन्द्रियों की चेतना में प्रकट होती है, यही बात हमने अपः नाम प्राणोदक के वर्णन में पायी है। हमने देखा कि महत् तत्व किस प्रकार सिन्धु सरस्वती होकर हमारी सभी चेतना-धाराओं को बीज रूप में धारण किये हुए तिस्र देवीः नामक इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति की त्रिविधता को प्राप्त करके हमारी समस्त चित्तवृत्तियों संकल्पों-विकल्पों और क्रियाओं के रूप में नानात्व ग्रहण करती है। यही सरस्वती नामक मूल चेतनधारा अहंकार रूप वृत्र का वध करने के कारण वृत्रध्नी बनी और इसी ने सप्तविधा आपो देवीः को त्रिविधता प्रदान करके हमारे व्यक्ति के कण-कण में पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप हमारे अन्धकार लिप्त जीवात्मा को नई स्फूर्ति, नया जीवन और नया जन्म प्राप्त हुआ। ये दिव्य आपः हमारे सभी पापों, दुरितों और कल्मषों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए वैदिक साधना में ‘प्राणा वा आपः’ को याद रख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि पूरे शोध प्रबन्ध में उदकनामों की चर्चा करते हुए आपः का उल्लेख किसी न किसी रूप में सर्वत्र प्राप्त हो जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि प्राणोदक का सर्वश्रेष्ठ नाम आपः ही है, परन्तु इन आपः को ऊपर से लाने का श्रेय उदंचनशील प्राणों को ही जाता है। अतएव निघंटु ने आपः शब्द को उदकनामों के अन्तर्गत ही रखा है और हम भी आगे उदकनामों के सन्दर्भ में ही विषय प्रस्तुत करते रहेंगे।
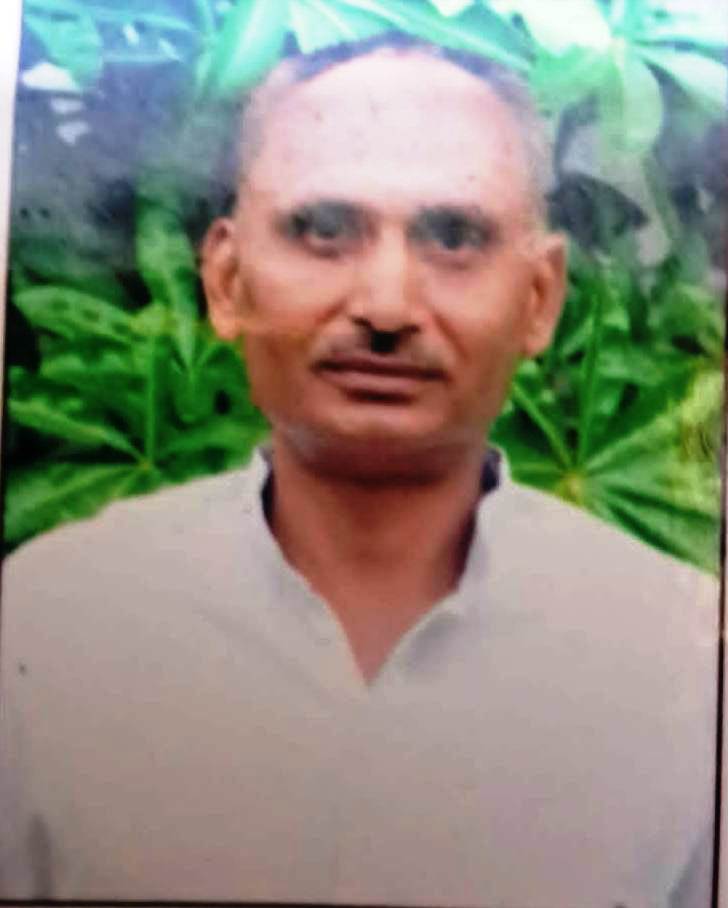
![]()
[1] प्राणा वा आपः - तैब्रा. ३.२.५.२,
अथो यदेवैनमेतदस्माल्लोकात्प्रेतं चित्यामादधत्यथो या एवैता अवोक्षणीया आपस्ता एव स ततोऽनुसं भवति प्राणं वेव प्राणो ह्यापः - जैउब्रा. ३.२.५.९
[3] आपो वा इदमग्रे महत्सलिलमासीत् स ऊर्मिरूर्मिमस्कन्दत्ततो हिरण्मयौ कुक्ष्यौ समभवतां ते एवर्क्सामे-जै.उ.ब्रा. १.१८.१.१
[4]
समुद्रज्येष्ठाः
सलिलस्य
मध्यात्पुनाना
यन्त्यनिविशमानाः
।
इन्द्रो
या
वज्री
वृषभो
रराद
ता
आपो
देवीरिह
मामवन्तु
॥ऋ.
७.४९.१
[5]
दूरे
तन्नाम
गुह्यं
पराचैर्यत्त्वा
भीते
अह्वयेतां
वयोधै
।
उदस्तभ्नाः
पृथिवीं
द्यामभीके
भ्रातुः
पुत्रान्मघवन्तित्विषाणः
॥१०.५५.१,
तु नामानि
नामानि
ते
शतक्रतो
विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे
।
इन्द्राभिमातिषाह्ये
॥ऋ.
३.३७.३, ३.५५.१०,
प्र व एते सुयुजो यामन्निष्टये नीचीरमुष्मै यम्य ऋतावृधः ।
सुयन्तुभिः सर्वशासैरभीशुभिः क्रिविर्नामानि प्रवणे मुषायति ॥५.४४.४,
पदं
देवस्य
नमसा
व्यन्तः
श्रवस्यवः
श्रव
आपन्नमृक्तम्
।
नामानि
चिद्दधिरे
यज्ञियानि
भद्रायां
ते
रणयन्त
संदृष्टौ
॥६.१.४
इत्यादि।
[6]
गौरीर्मिमाय
सलिलानि
तक्षत्येकपदी
द्विपदी
सा
चतुष्पदी
।
अष्टापदी
नवपदी
बभूवुषी
सहस्राक्षरा
परमे
व्योमन्
॥१.१६४.४१
[7]तस्याः
समुद्रा
अधि
वि
क्षरन्ति
तेन
जीवन्ति
प्रदिशश्चतस्रः
।
ततः
क्षरत्यक्षरं
तद्विश्वमुप
जीवति
॥
१.१६४.४२
[8] ज्योतिष्मतीम् उत्तमां उप दधाति तस्मात् प्राणानां वाग् ज्योतिर् उत्तमाः । - तैसं. ५.३.२.३
अनुष्टुभोत्तमया जुहोति वाग् वा अनुष्टुप् तस्मात् प्राणानां वाग् उत्तमा । तै.सं. ५.१.९.१, वाग् वा अनुष्टुप् तस्मात् प्राणानां वाग् उत्तमा - तैसं ६.६.११.६
[10] यत्रैतं प्राणा ऋषयोऽग्रेऽग्निं समस्कुर्वंस्तदस्मिन्नेतं पुरस्ताद्भागमकुर्वत -माश ७.२.३.५, प्राणा वै स्तोमाः प्राणा उ वा ऋषय – माश ८.४.१.६
(तु प्राणा वा ऋषयो देव्यासस्तनूपावान - ऐब्रा २.२७, माश ६.१.१.१,
प्राणा वा ऋषयः प्रथमजास्तद्धि ब्रह्म प्रथमजं – माश ८.६.१.५,
प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति – माश १४.५.२.५
[13]
इयं
मे
नाभिरिह
मे
सधस्थमिमे
मे
देवा
अयमस्मि
सर्वः
।
द्विजा
अह
प्रथमजा
ऋतस्येदं
धेनुरदुहज्जायमाना
॥
१०.६१.१९
[14]
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां
काष्ठानां
मध्ये
निहितं
शरीरम्
।
वृत्रस्य
निण्यं
वि
चरन्त्यापो
दीर्घं
तम
आशयदिन्द्रशत्रुः
॥ऋ.
१.३२.१०
[15]
को
ददर्श
प्रथमं
जायमानमस्थन्वन्तं
यदनस्था
बिभर्ति
।
भूम्या
असुरसृगात्मा
क्व
स्वित्को
विद्वांसमुप
गात्प्रष्टुमेतत्
॥१.१६४.४
[16]यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत् अन्योऽन्यज्जिघ्रेदन्योऽन्यद्रसयेत् अन्योऽन्यद्वदेदन्योऽन्यच्छृणुयात् अन्योऽन्यन्मन्वीत अन्योऽन्यत्स्पृशेदन्योऽन्यद्विजानीयात् ॥ बृहदार. ४.३.३१
[17]
ऋभुक्षणो
वाजा
मादयध्वमस्मे
नरो
मघवानः
सुतस्य
।
आ
वोऽर्वाचः
क्रतवो
न
यातां
विभ्वो
रथं
नर्यं
वर्तयन्तु
॥७.४८.१
[18]
सूरश्चिद्रथं
परितक्म्यायां
पूर्वं
करदुपरं
जूजुवांसम्
।
भरच्चक्रमेतशः
सं
रिणाति
पुरो
दधत्सनिष्यति
क्रतुं
नः
॥५.३१.११
[21]
अधाकृणोः
प्रथमं
वीर्यं
महद्यदस्याग्रे
ब्रह्मणा
शुष्ममैरयः
।
रथेष्ठेन
हर्यश्वेन
विच्युताः
प्र
जीरयः
सिस्रते
सध्र्यक्पृथक्
॥२.१७.३
[22]
उषसः
पूर्वा
अध
यद्व्यूषुर्महद्वि
जज्ञे
अक्षरं
पदे
गोः
।
व्रता
देवानामुप
नु
प्रभूषन्महद्देवानामसुरत्वमेकम्
॥१॥
मो
षू
णो
अत्र
जुहुरन्त
देवा
मा
पूर्वे
अग्ने
पितरः
पदज्ञाः
।
पुराण्योः
सद्मनोः
केतुरन्तर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्
॥३.५५.१-२
[23]
तद्देवस्य
सवितुर्वार्यं
महद्वृणीमहे
असुरस्य
प्रचेतसः
।
छर्दिर्येन
दाशुषे
यच्छति
त्मना
तन्नो
महाँ
उदयान्देवो
अक्तुभिः
॥४.५३.१
[26]महत्तत्सोमो
महिषश्चकारापां
यद्गर्भोऽवृणीत
देवान्
।
अदधादिन्द्रे
पवमान
ओजोऽजनयत्सूर्ये
ज्योतिरिन्दुः
॥
९.९७.४१
[27]
यदुष
औच्छः
प्रथमा
विभानामजनयो
येन
पुष्टस्य
पुष्टम्
।
यत्ते
जामित्वमवरं
परस्या
महन्महत्या
असुरत्वमेकम्
॥१०.५५.४
[29] यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् । सञ्ज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिधृर्तिमतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति । सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥-ऐ.उ ३.४
[30]
द्रप्सश्चस्कन्द
प्रथमाँ
अनु
द्यूनिमं
च
योनिमनु
यश्च
पूर्वः
।
समानं
योनिमनु
संचरन्तं
द्रप्सं
जुहोम्यनु
सप्त
होत्राः
॥१०.१७.११
[31]
आपो
यं
वः
प्रथमं
देवयन्त
इन्द्रपानमूर्मिमकृण्वतेळः
।
तं
वो
वयं
शुचिमरिप्रमद्य
घृतप्रुषं
मधुमन्तं
वनेम
॥७.४७.१
[32]सरस्वतीं
यां
पितरो
हवन्ते
दक्षिणा
यज्ञमभिनक्षमाणाः
।
सहस्रार्घमिळो
अत्र
भागं
रायस्पोषं
यजमानेषु
धेहि
॥
१०.१७.९
[33]
द्रप्सश्चस्कन्द
प्रथमाँ
अनु
द्यूनिमं
च
योनिमनु
यश्च
पूर्वः
।
समानं
योनिमनु
संचरन्तं
द्रप्सं
जुहोम्यनु
सप्त
होत्राः
॥१०.१७.११
[34]यस्य
त्वमग्ने
अध्वरं
जुजोषो
देवो
मर्तस्य
सुधितं
रराणः
।
प्रीतेदसद्धोत्रा
सा
यविष्ठासाम
यस्य
विधतो
वृधासः
॥
४.२.१०
[36]
धिया
चक्रे
वरेण्यो
भूतानां
गर्भमा
दधे
।
दक्षस्य
पितरं
तना
॥९॥
नि
त्वा
दधे
वरेण्यं
दक्षस्येळा
सहस्कृत
।
अग्ने
सुदीतिमुशिजम्
॥-
ऋ.
३.२७.९-१०
[37]
इडायास्पदं
घृतवत्सरीसृपं
जातवेदः
प्रति
हव्या
गृभाय
।
ये
ग्राम्याः
पशवो
विश्वरूपास्तेषां
सप्तानां
मयि
रन्तिरस्तु
॥-
अथर्व
३.१०.६
[38]अधा
होता
न्यसीदो
यजीयानिळस्पद
इषयन्नीड्यः
सन्
।
तं
त्वा
नरः
प्रथमं
देवयन्तो
महो
राये
चितयन्तो
अनु
ग्मन्
॥
ऋ.
६.१.२
[39]
समुद्रज्येष्ठाः
सलिलस्य
मध्यात्पुनाना
यन्त्यनिविशमानाः
।
इन्द्रो
या
वज्री
वृषभो
रराद
ता
आपो
देवीरिह
मामवन्तु
॥
७.४९.१
[40]
बृहतः
परि
सामानि
षष्ठात्पञ्चाधि
निर्मिता
।
बृहद्बृहत्या
निर्मितं
कुतोऽधि
बृहती
मिता
॥४॥
बृहती
परि
मात्राया
मातुर्मात्राधि
निर्मिता
।
माया
ह
जज्ञे
मायाया
मायाया
मातली
परि
॥-अथर्व
८.९.४-५
[41] वही
[42] वही
[43]
यानि
त्रीणि
बृहन्ति
येषां
चतुर्थं
वियुनक्ति
वाचम्
।
ब्रह्मैनद्विद्यात्तपसा
विपश्चिद्यस्मिन्न्
एकं
युज्यते
यस्मिन्न्
एकम्
॥-शौअ
८.९.३
[44]
षट्
त्वा
पृच्छाम
ऋषयः
कश्यपेमे
त्वं
हि
युक्तं
युयुक्षे
योग्यं
च
।
विराजमाहुर्ब्रह्मणः
पितरं
तां
नो
वि
धेहि
यतिधा
सखिभ्यः
॥-
शौअ
८.९.७
[45]
उषो
यदद्य
भानुना
वि
द्वारावृणवो
दिवः
।
प्र
नो
यच्छतादवृकं
पृथु
च्छर्दिः
प्र
देवि
गोमतीरिषः
॥१.४८.१५,
अयमु
ते
सरस्वति
वसिष्ठो
द्वारावृतस्य
सुभगे
व्यावः
।
वर्ध
शुभ्रे
स्तुवते
रासि
वाजान्यूयं
पात
स्वस्तिभिः
सदा
नः
॥७.९५.६
[46]
सप्तभिः
पुत्रैरदितिरुप
प्रैत्पूर्व्यं
युगम्
।
प्रजायै
मृत्यवे
त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत्
॥१०.७२.९
[47]
वृषायमाणोऽवृणीत
सोमं
त्रिकद्रुकेष्वपिबत्सुतस्य
।
आ
सायकं
मघवादत्त
वज्रमहन्नेनं
प्रथमजामहीनाम्
॥३॥
यदिन्द्राहन्प्रथमजामहीनामान्मायिनाममिनाः
प्रोत
मायाः
।
आत्सूर्यं
जनयन्द्यामुषासं
तादीत्ना
शत्रुं
न
किला
विवित्से
॥१.३२.३-४
[48]
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां
काष्ठानां
मध्ये
निहितं
शरीरम्
।
वृत्रस्य
निण्यं
वि
चरन्त्यापो
दीर्घं
तम
आशयदिन्द्रशत्रुः
॥१.३२.१०
[49]त्वं
ह
त्यदिन्द्रारिषण्यन्दृळ्हस्य
चिन्मर्तानामजुष्टौ
।
व्यस्मदा
काष्ठा
अर्वते
वर्घनेव
वज्रिञ्छ्नथिह्यमित्रान्
॥
१.६३.५
[50]
प्र
नू
महित्वं
वृषभस्य
वोचं
यं
पूरवो
वृत्रहणं
सचन्ते
।
वैश्वानरो
दस्युमग्निर्जघन्वाँ
अधूनोत्काष्ठा
अव
शम्बरं
भेत्
॥१.५९.६
[51]त्वामिद्धि
हवामहे
साता
वाजस्य
कारवः
।
त्वां
वृत्रेष्विन्द्र
सत्पतिं
नरस्त्वां
काष्ठास्वर्वतः
॥
६.४६.१
[52]
इमं
तं
पश्य
वृषभस्य
युञ्जं
काष्ठाया
मध्ये
द्रुघणं
शयानम्
।
येन
जिगाय
शतवत्सहस्रं
गवां
मुद्गलः
पृतनाज्येषु
॥१०.१०२.९
[53]उपो
ह
यद्विदथं
वाजिनो
गुर्धीभिर्विप्राः
प्रमतिमिच्छमानाः
।
अर्वन्तो
न
काष्ठां
नक्षमाणा
इन्द्राग्नी
जोहुवतो
नरस्ते
॥
७.९३.३
[56]
तुरीयं
नाम
यज्ञियं
यदा
करस्तदुश्मसि
।
आदित्पतिर्न
ओहसे
॥८.८०.९
(तु. यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् अथर्व
८.९.३
[57]यद्देवा
यतयो
यथा
भुवनान्यपिन्वत
।
अत्रा
समुद्र
आ
गूळ्हमा
सूर्यमजभर्तन
॥७॥
अष्टौ
पुत्रासो
अदितेर्ये
जातास्तन्वस्परि
।
देवाँ
उप
प्रैत्सप्तभिः
परा
मार्ताण्डमास्यत्
॥
१०.७२.७-८
[58]
सप्तभिः
पुत्रैरदितिरुप
प्रैत्पूर्व्यं
युगम्
।
प्रजायै
मृत्यवे
त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत्
॥१०.७२.९
[59]
आपो
ह
यद्बृहतीर्विश्वमायन्गर्भं
दधाना
जनयन्तीरग्निम्
।
ततो
देवानां
समवर्ततासुरेकः
कस्मै
देवाय
हविषा
विधेम
॥१०.१२१.७
[60]यश्चिदापो
महिना
पर्यपश्यद्दक्षं
दधाना
जनयन्तीर्यज्ञम्
।
यो
देवेष्वधि
देव
एक
आसीत्कस्मै
देवाय
हविषा
विधेम
॥
१०.१२१.८
[61]
अष्ट
जाता
भूता
प्रथमजा
ऋतस्याष्टेन्द्र
ऋत्विजो
दैव्या
ये
।
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमीं
रात्रिमभि
हव्यमेति
॥
-
अ
८.९.२१
[62] वही
[64]केवलीन्द्राय
दुदुहे
हि
गृष्टिर्वशं
पीयूषं
प्रथमं
दुहाना
।
अथातर्पयच्चतुरश्चतुर्धा
देवान्
मनुष्यानसुरान्
उत
ऋषीन्
॥-
अथर्व
८.९.२४
[65]
आपो
यं
वः
प्रथमं
देवयन्त
इन्द्रपानमूर्मिमकृण्वतेळः
।
तं
वो
वयं
शुचिमरिप्रमद्य
घृतप्रुषं
मधुमन्तं
वनेम
॥७.४७,
१
[66]
स
नो
देव
देवताते
पवस्व
महे
सोम
प्सरस
इन्द्रपानः
।
कृण्वन्नपो
वर्षयन्द्यामुतेमामुरोरा
नो
वरिवस्या
पुनानः
॥
ऋ
९.९६.३,
पवस्व
सोम
मधुमाँ
ऋतावापो
वसानो
अधि
सानो
अव्ये
।
अव
द्रोणानि
घृतवान्ति
सीद
मदिन्तमो
मत्सर
इन्द्रपानः
॥
९.९६.१३
[67] ९.९६.३
[68]
सोमः
पवते
जनिता
मतीनां
जनिता
दिवो
जनिता
पृथिव्याः
।
जनिताग्नेर्जनिता
सूर्यस्य
जनितेन्द्रस्य
जनितोत
विष्णोः
॥९.९६.५
[69]स
पूर्व्यो
वसुविज्जायमानो
मृजानो
अप्सु
दुदुहानो
अद्रौ
।
अभिशस्तिपा
भुवनस्य
राजा
विदद्गातुं
ब्रह्मणे
पूयमानः
॥
९.९६.१०
[70]इयमेव
सा
या
प्रथमा
व्यौच्छदास्वितरासु
चरति
प्रविष्टा
।
महान्तो
अस्यां
महिमानो
अन्तर्वधूर्जिगाय
नवगज्जनित्री
॥
अ
८.९.११
[71] वही
[72] ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में इन्द्रः आत्मा वा, ऋ. ४.२६ की देवता मानी गई है, ४.२७ और ४.१८ में भी विषय की समानता देखते हुए यही स्थिति माननी पडेगी।
[73]
गर्भे
नु
सन्नन्वेषामवेदमहं
देवानां
जनिमानि
विश्वा
।
शतं
मा
पुर
आयसीररक्षन्नध
श्येनो
जवसा
निरदीयम्
॥ऋ
४,२७.१
[74] एकैव वा महान् आत्मा – तद्विभूतयो अन्याः देवताः। ऋ. सर्वानुक्रमणी
[75]
पाकः
पृच्छामि
मनसाविजानन्देवानामेना
निहिता
पदानि
।
वत्से
बष्कयेऽधि
सप्त
तन्तून्वि
तत्निरे
कवय
ओतवा
उ
॥१.१६४.५
[76]यो
यज्ञो
विश्वतस्तन्तुभिस्तत
एकशतं
देवकर्मेभिरायतः
।
इमे
वयन्ति
पितरो
य
आययुः
प्र
वयाप
वयेत्यासते
तते
॥
१०.१३०.१
[77]
पुमाँ
एनं
तनुत
उत्कृणत्ति
पुमान्वि
तत्ने
अधि
नाके
अस्मिन्
।
इमे
मयूखा
उप
सेदुरू
सदः
सामानि
चक्रुस्तसराण्योतवे
॥१०.१३०.२
[78]गर्भे
नु
सन्नन्वेषामवेदमहं
देवानां
जनिमानि
विश्वा
।
शतं
मा
पुर
आयसीररक्षन्नध
श्येनो
जवसा
निरदीयम्
॥
४.२७.१
[79]अहं
भूमिमददामार्यायाहं
वृष्टिं
दाशुषे
मर्त्याय
।
अहमपो
अनयं
वावशाना
मम
देवासो
अनु
केतमायन्
॥२॥
अहं
पुरो
मन्दसानो
व्यैरं
नव
साकं
नवतीः
शम्बरस्य
।
शततमं
वेश्यं
सर्वताता
दिवोदासमतिथिग्वं
यदावम्
॥
४.२६.२-३
[80]
सप्तापो
देवीः
सुरणा
अमृक्ता
याभिः
सिन्धुमतर
इन्द्र
पूर्भित्
।
नवतिं
स्रोत्या
नव
च
स्रवन्तीर्देवेभ्यो
गातुं
मनुषे
च
विन्दः
॥१०.१०४.८
[81]
अच्छा
सिन्धुं
मातृतमामयासं
विपाशमुर्वीं
सुभगामगन्म
।
वत्समिव
मातरा
संरिहाणे
समानं
योनिमनु
संचरन्ती
॥३.३३.३
[82]
कुवित्सस्य
प्र
हि
व्रजं
गोमन्तं
दस्युहा
गमत्
।
शचीभिरप
नो
वरत्
॥२४॥
इमा
उ
त्वा
शतक्रतोऽभि
प्र
णोनुवुर्गिरः
।
इन्द्र
वत्सं
न
मातरः
॥६.४५.२४-२५.
वज्रमेको बिभर्ति हस्त आहितं तेन वृत्राणि जिघ्नते ॥८.२९.४,
सरस्वती
सरयुः
सिन्धुरूर्मिभिर्महो
महीरवसा
यन्तु
वक्षणीः
।
देवीरापो
मातरः
सूदयित्न्वो
घृतवत्पयो
मधुमन्नो
अर्चत
॥१०.६४.९
[84]
इयं
मे
नाभिरिह
मे
सधस्थमिमे
मे
देवा
अयमस्मि
सर्वः
।
द्विजा
अह
प्रथमजा
ऋतस्येदं
धेनुरदुहज्जायमाना
॥१०.६१.१९
[85]
अष्ट
जाता
भूता
प्रथमजा
ऋतस्याष्टेन्द्र
ऋत्विजो
दैव्या
ये
।
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमीं
रात्रिमभि
हव्यमेति
॥अ
८.९.२१
[87]
प्राग्नये
तवसे
भरध्वं
गिरं
दिवो
अरतये
पृथिव्याः
।
यो
विश्वेषाममृतानामुपस्थे
वैश्वानरो
वावृधे
जागृवद्भिः
॥१॥
पृष्टो
दिवि
धाय्यग्निः
पृथिव्यां
नेता
सिन्धूनां
वृषभ
स्तियानाम्
।
स
मानुषीरभि
विशो
वि
भाति
वैश्वानरो
वावृधानो
वरेण
॥२॥७.५.१-२
[88]
प्र
ब्रह्माणि
नभाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरज्यत
।
या
सप्तबुध्नमर्णवं
जिह्मबारमपोर्णुत
इन्द्र
ईशान
ओजसा
नभन्तामन्यके
समे
॥८.४०.५
[89] इस यज्ञ को प्राञ्च यज्ञ भी कहते हैं, जहां सोम का अद्रि भी है ।
प्राञ्चं
यज्ञं
चकृम
वर्धतां
गीः
समिद्भिरग्निं
नमसा
दुवस्यन्
।
दिवः
शशासुर्विदथा
कवीनां
गृत्साय
चित्तवसे
गातुमीषुः
॥
३.१.२
[90]
इन्द्र
उक्थेन
शवसा
परुर्दधे
बृहस्पते
प्रतरीतास्यायुषः
।
यज्ञो
मनुः
प्रमतिर्नः
पिता
हि
कमा
सर्वतातिमदितिं
वृणीमहे
॥१०.१००,
५
[91]
समिद्धो
अद्य
मनुषो
दुरोणे
देवो
देवान्यजसि
जातवेदः
।
आ
च
वह
मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं
दूतः
कविरसि
प्रचेताः
॥१०.११०.१
[93]यो
अग्निः
सप्तमानुषः
श्रितो
विश्वेषु
सिन्धुषु
।
तमागन्म
त्रिपस्त्यं
मन्धातुर्दस्युहन्तममग्निं
यज्ञेषु
पूर्व्यं
नभन्तामन्यके
समे
॥
८.३९.८
[95]
स्वश्वा
सिन्धुः
सुरथा
सुवासा
हिरण्ययी
सुकृता
वाजिनीवती
।
ऊर्णावती
युवतिः
सीलमावत्युताधि
वस्ते
सुभगा
मधुवृधम्
॥१०.७५.८
[96]
न
वा
उ
एतन्म्रियसे
न
रिष्यसि
देवाँ
इदेषि
पथिभिः
सुगेभिः
।
हरी
ते
युञ्जा
पृषती
अभूतामुपास्थाद्वाजी
धुरि
रासभस्य
॥१.१६२.२१
[97]ऋजीत्येनी
रुशती
महित्वा
परि
ज्रयांसि
भरते
रजांसि
।
अदब्धा
सिन्धुरपसामपस्तमाश्वा
न
चित्रा
वपुषीव
दर्शता
॥
१०.७५.७
[98]
सुखं
रथं
युयुजे
सिन्धुरश्विनं
तेन
वाजं
सनिषदस्मिन्नाजौ
।
महान्ह्यस्य
महिमा
पनस्यतेऽदब्धस्य
स्वयशसो
विरप्शिनः
॥१०.७५.९
[99]
आ
यत्साकं
यशसो
वावशानाः
सरस्वती
सप्तथी
सिन्धुमाता
।
याः
सुष्वयन्त
सुदुघाः
सुधारा
अभि
स्वेन
पयसा
पीप्यानाः
॥७.३६.६
[100]एकाचेतत्सरस्वती
नदीनां
शुचिर्यती
गिरिभ्य
आ
समुद्रात्
।
रायश्चेतन्ती
भुवनस्य
भूरेर्घृतं
पयो
दुदुहे
नाहुषाय
॥
७.९५.२
[101]चोदयित्री
सूनृतानां
चेतन्ती
सुमतीनाम्
।
यज्ञं
दधे
सरस्वती
॥११॥
महो
अर्णः
सरस्वती
प्र
चेतयति
केतुना
।
धियो
विश्वा
वि
राजति
॥
१.३.११-१२
[102]उषो
यदद्य
भानुना
वि
द्वारावृणवो
दिवः
।
प्र
नो
यच्छतादवृकं
पृथु
च्छर्दिः
प्र
देवि
गोमतीरिषः
॥
१.४८.१५
[104] वही
[105]
अप
नः
शोशुचदघमग्ने
शुशुग्ध्या
रयिम्
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥१॥
सुक्षेत्रिया
सुगातुया
वसूया
च
यजामहे
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥२॥
प्र
यद्भन्दिष्ठ
एषां
प्रास्माकासश्च
सूरयः
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥३॥
प्र
यत्ते
अग्ने
सूरयो
जायेमहि
प्र
ते
वयम्
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥४॥
प्र
यदग्नेः
सहस्वतो
विश्वतो
यन्ति
भानवः
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥५॥
त्वं
हि
विश्वतोमुख
विश्वतः
परिभूरसि
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥६॥
द्विषो
नो
विश्वतोमुखाति
नावेव
पारय
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥७॥
स
नः
सिन्धुमिव
नावयाति
पर्षा
स्वस्तये
।
अप
नः
शोशुचदघम्
॥८॥१.९७.१-८
[107]समित्तमघमश्नवद्दुःशंसं
मर्त्यं
रिपुम्
।
यो
अस्मत्रा
दुर्हणावाँ
उप
द्वयुः
॥१४॥
पाकत्रा
स्थन
देवा
हृत्सु
जानीथ
मर्त्यम्
।
उप
द्वयुं
चाद्वयुं
च
वसवः
॥
८.१८.१४-१५
[108]
इयं
न
उस्रा
प्रथमा
सुदेव्यं
रेवत्सनिभ्यो
रेवती
व्युच्छतु
।
आरे
मन्युं
दुर्विदत्रस्य
धीमहि
स्वस्त्यग्निं
समिधानमीमहे
॥४॥
प्र
याः
सिस्रते
सूर्यस्य
रश्मिभिर्ज्योतिर्भरन्तीरुषसो
व्युष्टिषु
।
भद्रा
नो
अद्य
श्रवसे
व्युच्छत
स्वस्त्यग्निं
समिधानमीमहे
॥१०.३५.४-५
[109]
दिवस्पृथिव्योरव
आ
वृणीमहे
मातॄन्सिन्धून्पर्वताञ्छर्यणावतः
।
अनागास्त्वं
सूर्यमुषासमीमहे
भद्रं
सोमः
सुवानो
अद्या
कृणोतु
नः
॥२॥
द्यावा
नो
अद्य
पृथिवी
अनागसो
मही
त्रायेतां
सुविताय
मातरा
।
उषा
उच्छन्त्यप
बाधतामघं
स्वस्त्यग्निं
समिधानमीमहे
॥१०.३५.२-३
[110]
श्रेष्ठं
नो
अद्य
सवितर्वरेण्यं
भागमा
सुव
स
हि
रत्नधा
असि
।
रायो
जनित्रीं
धिषणामुप
ब्रुवे
स्वस्त्यग्निं
समिधानमीमहे
॥१०.३५.७
[111]
आ
भारती
भारतीभिः
सजोषा
इळा
देवैर्मनुष्येभिरग्निः
।
सरस्वती
सारस्वतेभिरर्वाक्तिस्रो
देवीर्बर्हिरेदं
सदन्तु
॥३.४,८
[112]
दिवो
वा
सानु
स्पृशता
वरीयः
पृथिव्या
वा
मात्रया
वि
श्रयध्वम्
।
उशतीर्द्वारो
महिना
महद्भिर्देवं
रथं
रथयुर्धारयध्वम्
॥१०.७०.५
[113]व्यचस्वतीरुर्विया
वि
श्रयन्तां
पतिभ्यो
न
जनयः
शुम्भमानाः
।
देवीर्द्वारो
बृहतीर्विश्वमिन्वा
देवेभ्यो
भवत
सुप्रायणाः
॥
१०.११०.५,
देवीर्द्वारो
वि
श्रयध्वं
सुप्रायणा
न
ऊतये
।
प्रप्र
यज्ञं
पृणीतन
॥५.५.५
[114]अविन्दद्दिवो
निहितं
गुहा
निधिं
वेर्न
गर्भं
परिवीतमश्मन्यनन्ते
अन्तरश्मनि
।
व्रजं
वज्री
गवामिव
सिषासन्नङ्गिरस्तमः
।
अपावृणोदिष
इन्द्रः
परीवृता
द्वार
इषः
परीवृताः
॥
१.१३०.३
[115]
वि
श्रयन्तामृतावृधो
द्वारो
देवीरसश्चतः
।
अद्या
नूनं
च
यष्टवे
॥१.१३.६,
वि
श्रयन्तामुर्विया
हूयमाना
द्वारो
देवीः
सुप्रायणा
नमोभिः
।
व्यचस्वतीर्वि
प्रथन्तामजुर्या
वर्णं
पुनाना
यशसं
सुवीरम्
॥२.३.५,
कुविन्नो
अग्निरुचथस्य
वीरसद्वसुष्कुविद्वसुभिः
काममावरत्
।
चोदः
कुवित्तुतुज्यात्सातये
धियः
शुचिप्रतीकं
तमया
धिया
गृणे
॥१.१४३.६
[116]
वि
श्रयन्तामुर्विया
हूयमाना
द्वारो
देवीः
सुप्रायणा
नमोभिः
।
व्यचस्वतीर्वि
प्रथन्तामजुर्या
वर्णं
पुनाना
यशसं
सुवीरम्
॥२.३.५
[118]आ
नो
यज्ञं
भारती
तूयमेत्विळा
मनुष्वदिह
चेतयन्ती
।
तिस्रो
देवीर्बर्हिरेदं
स्योनं
सरस्वती
स्वपसः
सदन्तु
॥
१०.११०.८
[119]
प्र
या
महिम्ना
महिनासु
चेकिते
द्युम्नेभिरन्या
अपसामपस्तमा
।
रथ
इव
बृहती
विभ्वने
कृतोपस्तुत्या
चिकितुषा
सरस्वती
॥६.६१.१३
